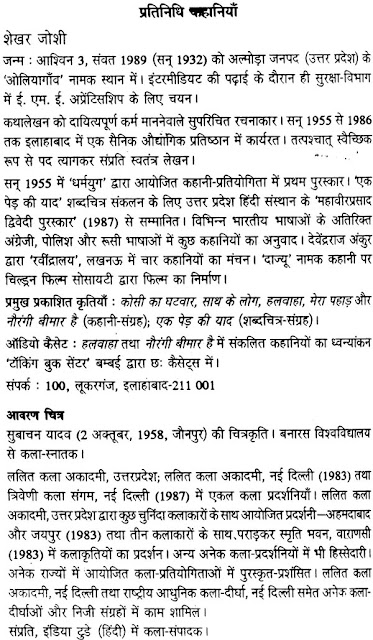शेखर जोशी की कहानी-बदबूः कुछ नोट्स
विमलेश त्रिपाठी
1.
बतौर एक कथाकार मैं कह सकता हूं कि एक
कहानी के लिए पठनीयता सबसे जरूरी चीज होती है – और यह पठनीयता साधाराण भाषा और
शैली से संभव नहीं होती बल्कि वह होती है पाठक के मन को स्पर्श करने की लेखकीय
क्षमता से। शेखर जोशी की कहानियां इस लिहाज से पठनीय हैं कि उन्हें पढ़ते हुए आप
उनकी मूल भावना से इस कदर जुड़ जाते हैं कि वह आपके अपने जीवन की कथा लगने लगती है
और यह न भी लगे तब भी उस कथा को आप कहीं गहरे पहचानते हैं, महसूस करते हैं। कथा
चाहे कितनी भी अलग और अछूते विषय को लेकर बुनी गई हो यदि पाठकों को स्पर्श करने की
क्षमता यदि उसके अंदर न हो तो वह कथाकार की असफलता की कथा होती है। बदबू कहानी में
इस तरह कमाल की पठनीयता है – कुछ इस तरह कि आप एक बार पढ़ना शुरू करें तो अंत तक
पढ़े बिना आपको चैन न मिले।
2.
बदबू की कथा मनुष्य के परिस्थितियों के
दास बन जाने की कथा नहीं है – हां यह जरूर है कि कथा में बहुतेरे लोग परिस्थिति के
दास की तरह चित्रित हुए हैं। बदबू के साथ उनका मानसिक और शारिरीक समझौता इस बात की
ओर संकेत करता है कि वे बदबू में रहने के आदी हो गए हैं – यह बदबू सिर्फ किरासन
तेल या कारखाने की गंदी कालिख की बदबू नहीं है बल्कि हमारे सड़े हुए तंत्र की भी
दुर्गंध है जिसके साथ हम आराम से अपना जीवन बसर कर रहे हैं और हमें बहुत खास कुछ
मलाल नहीं है, अगर है भी तो भय के वशीभूत हम उसे प्रकट करना नहीं चाहते। पूरी कथा में बदबू के ध्वन्यार्थ या
व्यंग्यार्थ को महसूस किया जा सकता है। यदि कारखाने को एक देश मान लिया जाए और
उसमें काम करने वाले लोगों को आम नागरिक तो एक बहुत ही मार्मिक बिंब उभर कर आता है
जो हमें सोचने के लिए बाध्य करता है।
3.
इस कहानी में तंत्र की साजिशें हैं – उस
एक आवाज के खिलाफ जो नायक की है। नायक कारखाने में नया आया है लेकिन वह अन्य लोगों
की तरह समझौता परस्त नहीं है – वह अन्याय के खिलाफ अवाज उठाता है – लोगों को एकत्र
करता है। कुछ लोग उसके साथ आते भी हैं लेकिन संगठन की खबर चीफ तक पहुंच जाती है और
वह नायक को कई तरह से समझाता-धमकाता है। यहां कारखाने में मजदूरों की जो अवस्था है
उसकी झलक मिलती है। साहब लोग दिन भर सिगरेट फूंकते हुए घूमते रहते हैं लेकिन एक
मजदूर जब छूपकर बीड़ी पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसपर जुर्माना लगा दिया जाता है –
सारे मजदूरों को बीड़ी न पीने की सख्त हिदायत दी जाती है। इस हिदायत के खिलाफ जब
कथा का नायक आवाज उठाता है तो चीफ की भौंहे तन जाती हैं और उसपर नजर रखी जाने लगती
है। इस देश के कारखाने में आज भी मजदूरों की अवस्था कमोबेश यही है – वे रातदिन जी
तोड़ मिहनत करने के बाद भी उचित मजदूरी प्राप्त नहीं कर पाते और उनके साथ ऐसे सलूक
किया जाता है जैसे वे आदमी न होकर कोई जीव हों जिनका जन्म ही मिहनत करने और चुपचाप
अन्याय सहने के लिए हुआ हो।
कहानी में तंत्र की साजिशें हैं तो उसके
खिलाफ उठने वाली आवाज भी है – कहानी में सिर्फ साजिशें होतीं और अंततः नायक का
बदबू के साथ समझौता कर लेने के दृश्य अकित होते तो मेरे लिहाज से यह कहानी बड़ी
कहानी नहीं बन पाती। कहानी का नायक कारखाने के अत्याचारी तंत्र के खिलाफ अकेले ही
आवाज उठाता है – वह वहां काम करने वाले लोगों को संगठित करना चाहता है, भले ही
उसके प्रयास विफल हो जाते हैं लेकिन उसके अंदर की मानवीयता और अन्याय के खिलाफ
विद्रोह करने की क्षमता का शमन नहीं हुआ है। कहानी में तंत्र की साजिशों के आगे
नायक एक जगह पर विवश दिखने लगता है, जो स्वाभाविक भी है लेकिन कहानी का अंत इस तरह
होना हमें गहरी आश्वस्ति से भर देता है – “दूसरी बार मिट्टी
लगाने से पहले उसने हाथों की सूंघा और अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है।
सहसा एक विचित्र आतंक से उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा आज वह भी घासी की तरह
इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि
वह एक बार फिर हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ मगर फिर बड़ी मुश्किल से
वह धीरे-धीरे दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा न रही...
पहली बार उसे भ्रम हुआ था। हाथों से कैरोसीन तेल की बदबू अब भी आ रही थी।” कहानी में यहां आकर बदबू का अर्थ बिल्कुल बदल
जाता है – यहां बदबू मनुष्य की उस जिजिविषा का प्रतीक बन जाता है जो विपरीत से
विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रहता है। यहां उद्धरित पंक्तियां नायक के समझौता न
करने की क्षमता को भी दर्शाने वाली पंक्तियां हैं जो कथा को एक पोजिटिव शेड देती
हैं।
5.
कथा में गरीबी के संकेत एक वाक्य खण्ड के
द्वारा मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त हुआ है – बबुआ की टोपी इस बार भी रह गई। कथाकार ने बस इतना भर कहलवाया है – वह डिटेल
में नहीं जाता। शेखर जोशी आनावश्यक डिटेल में जाने वाले कथाकार नहीं है – वे एक
वाक्य में कथा की एक बड़ी दुनिया क अभिव्यक्त करने की योग्यता रखने वाले कथाकार
हैं। वे कथा को आगे बढ़ाने के लिए छोटी-छोटी उप कथाओं का सहारा लेते हैं – बिट और
व्यंग्य का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वे सभी उनकी केन्द्रीय कथा को और अदिक
सुस्पष्ट और बनाने और धार देने के लिए होते हैं। इस कथा में भी घासी राम का एक
प्रसंग एक मजदूर के मुंह से कहलवाया गया है।
6.
शेखर जोशी की कहानियों के संवाद बेहद
चुटिले और संक्षिप्त हैं। उनके पात्र बहुत कम बोलकर अधिक अर्थों की अभिव्यक्ति
करते हैं – बदबू कहानी भी इसका अपवाद नहीं है। बबुआ की टोपी इस बार भी रह गई – इस
छोटे से संवाद में गरीबी-बेबशी और पीड़ा का एक पूरा संसार झलक उठता है।
*****
अनहद से साभार